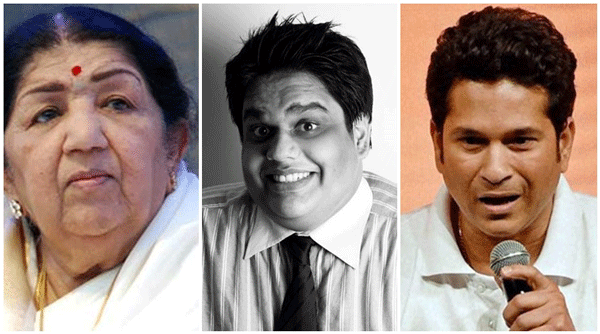सत्यदेव त्रिपाठी
संजू फिल्म संजय दत्त के जीवन के सिर्फ दो संवेदनशील मामलों को लेकर बनी है। जीवनी पर बनाने का इरादा होता, तो कम से कम उसकी शादी और पत्नी-बच्चों आदि की जरूरी बातें तो शामिल होतीं। लेकिन सिर्फ दो प्रसंगों को लेकर बनी इस फिल्म का निहित मकसद कुछ और है- श्री दत्त की आवारा और मुजरिम जिन्दगी को साफ-पाक सिद्ध करना। यदि पारिवारिक प्रसंग लेते, तो फिल्म में अनिवार्य रूप से बताना पड़ता कि जब संजू की परिणीता विदेश में पड़ी मौत से जूझ रही थी, वह यहां किसी और तारिका (माधुरी दीक्षित) के साथ रंगरेलियां मना रहा था। और यह सब उसकी चरित्रवानता के खिलाफ जाता। जाहिर है कि जीवन के सच पर बनी यह फिल्म कला के सच और जीवन के प्रति कला के सरोकार के भी विरुद्ध है।
संजू बाबा के जीवन की दोनों सच्ची घटनाएं हैं- उसका भयंकर नशेड़ी होना और गैर कानूनी ढंग से एके 47 जैसा खतरनाक हथियार रखना एवं बम-विस्फोट की घटना को जानते हुए भी छिपाना। अब अपने निहित रुझानों (वेस्टेड इंटरेस्ट्स) के तहत संजू के मित्र और इस फिल्म के निर्देशक राजकुमार हिरानी और उनकी मांग पर फिल्म के लेखक अभिजात जोशी उस जुर्म और गन्दी आदत को वाजिब कारणों से ढकने का प्रयत्न करते हैं। कारण खोजना और उसे सिद्ध करना ही फिल्म का प्रमुख उद्देश्य है। लेकिन दिये हुए कारण भी उतने वाजिब नहीं ठहरते, बल्कि बेहद फिल्मी लगते हैं। परंतु उससे बड़ा सवाल यह है कि वे कारण कितने भी सच होते, तो क्या उस कार्य को ढक सकते जो संजय दत्त ने किया, या उस वक्त उससे जो कुछ हुआ? कहा गया है कि ‘कारन ते कारज कठिन’। इतना बड़ा नर-संहार है वह कठिन कार्य, जो किसी भी कारण से ढका नहीं जा सकता। बेइंतहा नशेड़ी होने को एक गलत दोस्त के झांसे में ढका जाता है, जो उस मोहग्रस्त मां जैसी छाप देता है, जो अपने बेटे की हर गलती का जिम्मेदार बहू को बताकर संतुष्ट हो लेती है। और फिल्म ‘संजू’ तो संजय को दुनिया का हर ड्रग लेने वाला तथा साढ़े तीन सौ लड़कियों के साथ सम्बन्ध रखने वाला बताकर उसके नशेड़ीपने एवं अय्याशी को गोया गौरवान्वित करती है। जूते में ड्रग लेकर दो छोटी बहनों के साथ विमान में आ जाने को साहस (डेयरिंग) बताती है। और सारे हाथ-पांव मारने के बाद भी फिल्म उसके बचपने या बड़े घर के मनबढू बेटे होने के सिवा कोई खास कारण नहीं दे पाती। उधर महंगे इलाज के अलावा अनुशासनात्मक कुछ न करने वाले मां-बाप भी फिल्म(कारों) के अनजाने ही कटघरे में खड़े हो जाते हैं। मां की बीमारी को भुलाने के लिए नशा करना- ‘याद न आये दुखमय जीवन इससे पी लेता हाला’ कहां का माफीनामा (एक्सक्यूज) है? ऐसा होता, तब तो हर बीमार माता-पिता का बेटा नशेड़ी होता।
उधर कट्टरपंथियों द्वारा सांसद बाप को दी जाती धमकियों के चलते एके 47 रखने का कारण दिया जाता है। यदि नशे के लिए जिम्मेदार एक दोस्त था, तो जुर्म के लिए मीडिया को निशाना बना लिया गया है। मीडिया में शीर्षक के समक्ष सवालिया निशान की युक्ति (ट्रिक) का फिल्म में अच्छा इस्तेमाल हुआ है। अखबार वाले ऐसा करते हैं, पर ‘संजू’ के लिए वह कहावत ज्यादा सही है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता और यहां तो हथियार रखने और गैरेज में आपत्तिजनक सामान होने की बात संजय फिल्म में कुबूल भी करता है- कोर्ट में कर ही चुका है। मामला कुल मिलाकर यह कि संजय को अच्छा साबित करने के लिए बनी यह फिल्म यदि हिट हो रही है, तो कल हर बड़ा मुजरिम यह काम कर सकता है- विजय माल्या और नीरव मोदी तो कर ही सकते हैं। अब क्या कला के सरोकार यही रह गए हैं! इस तरह संजय को बचाने की रौ में उसे और बेपर्द (एक्सपोज) कर देती है फिल्म- खुद तो बेतरह होती ही है। क्योंकि कला का सच यह भी है कि यहां बोलना अपने को खोलना होता है- ‘शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे’।
और ऐसे देखा जाए, तो इस मकसद के लिए फिल्म बनाने की जरूरत ही नहीं थी। आम जनता की याददाश्त इतनी भुलक्कड़ होती है कि वह संजय की फिल्मों के बम्बइयापने के मजे (फन) में उसके जुर्म को भूल चुकी है। संजू बाबा भी मशक्कत और शान से पूरी सजाएं काट चुका है। बेजा पैरवी तो बाप ने नहीं की, हम सब जानते हैं, तो ये फिल्म वाले क्यों कर रहे हैं- ‘कुरेदते हो जो ये राख, जुस्तजू क्या है?’ झूठे ही उद्गारे दे रहे हो! और जिनके पास समझ है, उन्हें तो यह निहायत भावुक व अतिरंजनापूर्ण फिल्म बहला नहीं सकती। अस्पताल से भागकर उस अनजान शहर में इतनी दूर वह अमीरजादा पैदल व भीख मांगते हुए अपने दोस्त के पास पहुंच जाएगा… ऐसे गढ़े हुए दुस्साहस को वेद व्यास आके कहें, तो भी मानने की बात नहीं, हिरानी किस खेत की मूली हैं? उक्त मामलों से डगमगाये करियर को संभालने के लिए, संजय को लोकप्रिय और भला सिद्ध करते हुए उस वक्त भी संजय को एक बड़ा हथियार थमाया था फिल्म वालों ने ही- रुक्खों की छुट्टे सांड जैसी ‘बिन्धास’ जिन्दगी का। और बम्बइया शैली के बहाने मजेदार व चटपटी के नाम पर भ्रष्ट होती भाषा की सौगात अता की थी अवाम को। इनके दूरगामी परिणामों का किसी को ख्याल नहीं आ रहा है, जिसके लिए शायद इतिहास कभी न संजय दत्त को मुआफ कर पाएगा, न ही एमबीबीएस और लगे रहो मुन्ना भाई के बनाने-बनवाने वालों को। और वही लोग हैं, जो अब ‘संजू’ लेकर आये हैं- सफलताओं के नशे ने इन्हें भी मुन्ना भाई बना दिया है! मजे लेने और हंसाने जैसे मामूली व सस्ते (चीप) मकसद के लिए संस्कृति और भाषा को शृंखलाबद्ध रूप से विकृत करना किसी सभ्य नागरिकता का काम नहीं हो सकता।
लेकिन फिल्म की कला का न सही, फिल्म-उद्योग के दाम कमाने का काम हो सकता था… हुआ भी। मुन्ना से जो चस्का लगा, उसे अब ‘संजू’ से और भुनाने का मकसद अवश्य सध रहा है- दो हफ्ते में 300 करोड़ की रेकॉर्ड-तोड़ कमाई कर चुकी है फिल्म। ‘सलमान को पीछे छोड़ चुका है रनबीर कपूर’ की चर्चा की आड़ में फिल्मकारों की तिजोरी बढ़ रही है। पूछने का मन होता है- तोहरो तिजोरी कबौं भरिहैं की नाहीं, ए विधु विनोद चोपड़ा, ए राजकुमार हिरानी? यदि श्रेष्ठ जीवनीपरक का इरादा होता, तो दिलीपकुमार, देवानन्द व संजीव कुमार आदि सिनेमा के पौराणिकों (लीजेण्ड्स) पर पहले बनाते, लेकिन नयी पीढ़ी में उन्हें वो दर्शकता न मिलेगी कि ‘बाहुबली’ के विक्रय की बराबरी कर पाएं- वो तो संजू बाबा जैसी सस्ती लोकप्रियता के बल ही मिलेगी। अभी पिछले दिनों धोनी पर फिल्म बन गई, उसका करियर अभी चल रहा है और कपिलदेव-गावस्कर को कौन पूछता है- उनका खरीदार कौन है? वही हाल संजू बाबा का है। उसका बजार अभी बना हुआ है, तो बेच लो उसे- निभा लो दोस्ती भी- एक तीर से दो शिकार। दोस्त प्रीतीश नन्दी फिल्म देखने भी नहीं गये (संडे मेल), क्योंकि वे संजय को बेहतर जानते हैं- फिल्म के मोहताज नहीं, शायद फिल्म को भी जानते हों कि वो बताती कहां है, वो तो बेच रही है संजय को। और युग तो बिकने-बेचने का ही है- बाजार में बॉयोपिक बेचने की वृत्ति (ट्रेंड) है।
कहना यह भी होगा कि यहां संजय को बेदाग सिद्ध करने के निहित स्वार्थों के चलते फिल्म इतनी इकतरफा सरोकारविहीन व कला-विरोधी हो गई है, वरना ‘थ्री ईडियट्स’ के साक्ष्य पर हिरानी तो मास्टर हैं दोनो पक्षों के… और यदि संजय की जीवनी वाले व्यक्तिगत पक्ष को बाद करके एक आम कथा (फिक्शन) की तरह देखा जाए, तो बतौर फिल्म ‘संजू’ भी अपनी निर्मिति व प्रस्तुति में उतनी ही बेजोड़ है- हर कोण से सर्वांग सुन्दर। बस, जीवनी लिखते हुए डी.एन. त्रिपाठी नाम्ना लेखक (पीयूष शुक्ला) को बापू-बाबा के लिए मारते हुए फिल्म की शुरुआत लद्धड़है। लेकिन लिखने वाले की खोज के साथ फिल्म की शुरुआत और फिल्म के अंत में किताब तैयार की शैली बड़ी उर्वर बन पड़ी है। संवेदनाओं के साथ खेलने का गुर हिरानी को हासिल है। इसमें भी खूब खेले-खिले हैं- ऐसा कि कई बार आंखें भर-भर आती हैं। प्रेम और दोस्ती उनके पसन्दीदा विषय हैं, जिसे वे नाटकीयता व हास्य (कॉमेडी) भरे खिलन्दडेÞपन के साथ पेश करते हैं। इसे हिरानी का एल.सी.डी. (लाफ्टर-क्राइ-ड्रामा) कहते हैं। ईडियट्स थ्री थे, तो यहां भी दो हैं- संजू बाबा के साथ कमाली है। कमाली में वो पसन्दीदा गुजराती संस्पर्श (‘गुजू टच’) है। दोनों के बीच की ड्रामेबाजी में भावनाओं के ऐसे ज्वार उठते हैं कि दिल को थामना मुश्किल हो जाता है। भावात्मक रिश्ते को दृश्यों-संवादों की जुगलबन्दी वाली हिरानी-हथौटी यहां भी बदस्तूर है। कमाली की प्रेमिका के साथ संजू-सम्भोग में संजू की चरित्रहीनता का चरम है, पर यह और इसके समक्ष कमाली-जवाब अश्लील भी हो गए हैं। ‘गबागब’ का ईजाद विनोदी है, पर प्रयोग में श्लीलता भंग होती है। प्रतीकात्मक जुहाव के स्थल यूं कई हैं। संगीत पक्ष प्रभावहीन है।
कलाकारों के चयन में राजू हिरानी की खूबी क्या खूब है। संजू को मुन्ना भाई की छबि (इमेज) दी थी और रणबीर कपूर को ऐसा संजू बनाया है कि वह खुद भी रणबीर कपूर को भूल जाना चाहेगा। रणबीर के करियर का ग्राफ न कभी इतना ऊंचा उठा, न टिकिट खिड़की पर गिनती का। लेकिन हिरानी ने चुना व बताया भर होगा, चुने जाने लायक तो बनाया अपने को खुद रणबीर ने और वैसा बनने के लिए किया भी उसी ने। साफ कहंू तो फिल्म का सबसे उल्लेख्य पक्ष यही है। वरना कितने हिरानी हेरा जाते। कमाली के लिए विक्की कौशल को चुनने भर का कमाल ही है हिरानी का, वरना वह तो है ही कमाल- ‘राजी’ के अपेक्षाकृत दबे व छोटे किरदार में उसका कमाल ‘पालने में पूत के पांव’ जैसा लगा था। यहां ऐसी तस्दीक की, कि सब देखते रह गए। मनीषा को नरगिस दत्त के लिए चुना, तो वैसे दृश्य भी सिरजे कि वे नरगिस जैसा कर सकें। संजू की पहली कथित प्रेमिका की जैसी भद्द उड़ी होगी, उतनी उड़वाते हुए मेहमान भूमिका को सोनम कपूर ले उड़ी हैं। बेलगाम संजू के सामने मान्यता बनी दीया मिर्जा को शालीन होना ही था। पूरी फिल्म आत्मकथा न लिखने की जिद ठाने व वैसा कारण फाने अनुष्का गुड़िया भर (शो पीस) ही थीं, पर अंत तक आकर ‘कुछ न का कुछ’ हो गर्इं। पिता सुनील दत्त के रूप में परेश रावल के चयन व रूपायन का मामला विस्मयकारक है। कद-काठी मेल खाती नहीं, तो दिखने का सवाल ही न था, चलने-बोलने में उन्होंने परेश रावल ही रहना तय कर लिया, तो हिरानी क्या करते? वो तो भूमिका इतनी प्रभावी थी कि लोग परेश रावल को भूल गये। बोमन ईरानी के मूल किरदार की पहचान ही न थी और उन्हें तो बाजी मारनी ही थी। सब कुछ के साथ और सब कुछ के बावजूद इतने सारे कलात्मक सरंजामों में कसी और अकूत कमाइयों से भरी फिल्म ‘संजू’ कला-चेतना के बेजा इस्तेमाल के चलते बाबा तुलसी के शब्दों में ‘मन मलीन तन सुन्दर’ ही कही जा सकेगी।