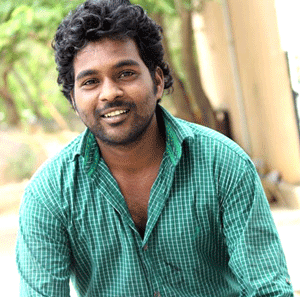सत्यदेव त्रिपाठी।
मुझसे दस साल बड़े इस मिस्त्री को सामने तो हम राजमन भइया कहते थे, पर आड़ में राजमन मिस्त्री या सिर्फ मिस्त्री भी कह लेते थे। दुकान पर जिन्दगी की पहली चाय मुझे राजमन भइया ने ही पिलाई थी और ठेकमा बजार में मन्दिर के सामने पाकड़ के पेड़ के नीचे की रामा हलवाई की दुकान और उस चाय तथा अनजाने में होंठ जल जाने के स्वाद की याद मुझे आज भी है। और याद है वह सीख भी, जो 1971 में मुम्बई जाते हुए उन्होंने मुझे दी थी- ‘सत्देव भइया, जैसे यहां सायकिलें चलती हैं, वैसे ही मुम्बई में मोटरें चलती हैं। संभाल के चलना और रोड पार करते हुए तो बहुतै सजग रहना…’। बावजूद इसके जब छह के महीने अन्दर ही कार से टकरा कर डेढ़ महीने सायन अस्पताल में रहा, तो हर क्षण मिस्त्री भइया को याद करता रहा। दसवीं में पढ़ते हुए जब घर-बार की सारी जिम्मेदारी अचानक मेरे कन्धों पर आ गई थी, तो 1968 से 71 तक राजमन भैया भी हमारे हीरो लोगों में एक हुआ करते थे।
तब तक वे मुम्बई से मिस्तिराना करके वापस आ चुके थे और ठेकमा में एक दुकान खोलकर अपना वही काम करने लगे थे। काम करते हुए गंजी पर लुंगी या तौलिया के बाने में रहने वाले राजमन भाई दुकान से बाहर चुनिया कर पहनी हुई धुली धोती पर सफेद या गाढ़े नीले रंग की पूरी बांह की कमीज पहनते थे। धोती पर कमीज और पांव में बूट या सैण्डिल का चलन (फैशन) तब शरीफाना माना जाता था और उनके लम्बे कद व मेहनत से पुष्ट बदन पर वह खूब फबता था। राजमन भइया अच्छी (सिंगापुरी) सायकल पर चलते थे और हल्के तेल लगे करीने से फिरे बाल हवा में लहराते हुए भी अपनी सेट जगह पर बैठे रहते थे। मुंह में पान और होठों पर जली हुई बीड़ी लिए (या लाइटर से फट-फट करके बीड़ी जलाते हुए) भी वे टकाटक आवाज व वाजिब लहजे में बोलते थे। उनकी बातों में एक अलग ही सोच व तर्क हुआ करता था, जिसे वे बहुत ठह के पेश भी करते थे। और यह सब मुझ किशोर को ही नहीं, बहुतों को बहुत भाता था। नतीजतन वे सड़क-दुकान-मकान कहीं भी हों, छोटी-बड़ी मजलिस उनके इर्द-गिर्द लगी रहती थी। और प्राइमरी तक भी न पढ़े-लिखे राजमनि मिस्त्री कई सभा-सोसाइटियों में बोलने के लिए बुलाए जाते। कुछ-कुछ नेता जैसा जल्वा था। लेकिन उनके मुरीदों के साथ मुखालिफों की तादाद भी कम न थी। पढ़ने-लिखने के बाद समझ में आया कि राजमन मिस्त्री का नाम असल में राजमणि विश्वकर्मा होना चाहिए, पर इस नाम से कोई आज भी उन्हें बताएगा नहीं।
और अब तो पिछले 15-18 सालों से कोई उनके पास जाता भी नहीं- विस्मयकारी है ऐसी मुख्य धारा का ऐसा हाशिया! अपनी सारी फिदाई और लगाव के बावजूद उनके पास जाने में मुझे एक पीड़ा भरा कुतूहल भी था उस ‘मजलिसी शख़्स के एकांत’ को देखने का। दाहिनी आंख तो उनकी उन्हीं दिनों चली गई थी- आग से धधकते लोहे पर पड़े जोरदार हथौडेÞ से छिटकी चिनगारी से। लेकिन बाद में बार्इं आंख भी जाती रही। पूरा अन्धा होने के बाद उनसे यह मेरी पहली मुलाकात थी। आस-पास का परिवेश पूरा बदल गया था, पर जामुन का पेड़ वही था और वही पुराना घर था, जिस पर पोती हुई मिट्टी कुछ नई थी। उनकी विशाल काया वैसी ही थी, किंतु न वह धज, न वह धार। लुंगी मात्र पर नंगे बदन सुर्ती मलते राजमन भइया को देखना पुराने पिंजरे में बसे नए वजूद को फिर से पहचानने जैसा था। राजमन भइया वही थे, पर न वह आक्रोश, न वह सक्रियता। असमंजस और अनहोनी की आशंका से भरी मेरी उत्तेजना की आग चरम पर थी, लेकिन राजमन भाई के धैर्य और हिम्मत ने उसका शमन कर दिया। देखते ही ‘का राजमन भैया, कैसे हउआ…’ की आतुर पुकार पर ‘अरे सत्देव भाई, आवा-आवा…’ के त्वरित हहास ने समय के बड़े अंतराल को पल भर में पूर दिया। जहां से छूटे थे, अनायास ही वहीं से शुरू होकर दो घंटे चले अनवरत संवादों के बीच पत्नी (मिस्त्री की तीसरी) की मदद से उनकी दतुअन होती रही, हम साथ-साथ चाय पीते रहे और जो कुछ सामने आया, वह उस पहले वाले राजमन मिस्त्री जैसा न था।
कैसी है तबियत, के जवाब में पहले ही संवाद को मैं सहसा समझ न पाया- ‘मुझे कोई रोग नहीं है, वो वही ससुरी है, जो ऐसा जकड़ लेती है कि पैर ही जमीन पर नहीं पड़ने देती…’। कुछ समय लगा समझने में कि उनका आशय भूतनी-प्रेतनी से था। राजमन जैसे प्रगतिशील सोच वाले से यह उम्मीद कतई न थी। लेकिन दो दशकों के अन्धकारमय जीवन ने ऐसे गहन कुहासे में धकेल दिया है। प्राय: अनपढ़ होने ने इसे आसान बना दिया होगा। कहां-कहां के ओझा-सोखा को दिखाने नहीं गए, पर किसी डॉक्टर के पास जाने के प्रश्न पर ‘डॉक्टर क्या करेगा’ की बाड़ लग गई है। अब किसी पूर्णमासी या अमावश्या को घर से 20 किलोमीटर पश्चिम खुटहन के पास किसी गांव में इस विश्वास के साथ जाने की फिराक में हैं कि वह उसी दिन ठीक ही कर देगा। हिम्मत उनकी कि किसी की बाइक पर एक किलोमीटर दूर बस स्टैण्ड तक सुबह-सुबह ही जाते हैं। वहां से जाने वाली एकमात्र बस से ठेकमा जाके बस बदलना या फिर बस की दिशा में जहां तक जा सकें… के अनुसार अभी आ-जा लेते हैं।
मेरी चिंता और जिज्ञासा दूसरी आंख के खराब होने के मामले को लेकर थी, जिसमें न जाने कहां से खून का थक्का उतरा, जिसे यहां से दिल्ली तक के डॉक्टरों ने पुतली के ऊपर समझा, लेकिन बहुत पता करने के बाद जब हिम्मत करके दिल्ली के कीर्त्ति नगर में स्थित किसी डॉ. कॉलरा से आॅपरेशन कराया, तो पंद्रह दिनों तक दर्द और दर्द-नाशक की आंखमिचौली के बाद आखिर दूसरी आंख भी जाती रही। लेकिन भला हो हमारी पारम्परिक व्यवस्था का कि सुबह उठने से रात को सोने तक हर नित्य क्रिया के लिए सहर्ष कोई न कोई तैयार रहता है। जिन्दगी आराम से चल जा रही है, वरना सब अंग दुरुस्त मां-पिता को मात्र दो जून दो-दो रोटी न दे सकने वाला हमारा प्रगत व बेहद सम्पन्न समाज वृद्धाश्रम भेज दे रहा है। राजमनि भइया की इस घोर त्रासदी में यह एक बेफिक्री है, उनके एकांत को असह्य नहीं होने देती।
बड़ा बेटा कुछ ज्यादा मोटी बुद्धि का है, जिसे निर्देश देकर चार बीघा पुस्तैनी खेती करा लेते हैं। और शेष कमी मुम्बई में अपनी लोहारगीरी के काम से छोटा बेटा पूरी कर देता है। छोटे बेटे के बच्चे और बेटी का एक बच्चा यानी नाती-पोते हमारी पारम्परिक संस्कृति के बिना टिकिट मंसायन हैं। लेकिन तरस आता है कि अपने समय के इतने समझदार, गुनी व कर्मठ राजमन भइया अपने नामी कारीगर पिता तिरसू दादा के बनाए घर व खेती में कोई इजाफा नहीं कर पाए। लेकिन बातचीत से लगा कि आज भी वे अपनी दर पर सिमटे होने के बावजूद अपने गांव (बड़ेपुर) ही नहीं, आस-पास के गांवों तक प्राय: सबकी खबर रखते हैं। और यह सूचना ही उनकी अंधेरी दुनिया का आलोक है। सबके साथ होने का भाव (फील) है और है उनका वह पुराना जीवट, जिसके सहारे वे ‘न दैन्यं, न पलायनं’ के पुरुषार्थ को जी रहे हैं। इस अदम्य जिजीविषा को नमन!