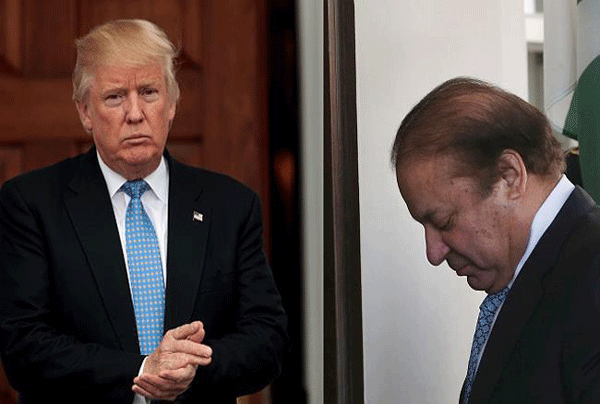सत्यदेव त्रिपाठी
दिल्ली के एक बड़े होटल में प्रशिक्षण-वृत्ति (इंटर्नशिप) कर रहे होटल प्रबंधन के छात्र-समूह में से एक लड़की शिउली चौथी मंजिल से नीचे गिरकर लंबी बेहोशी की हालत (कोमा) में चली जाती है। बाद में पता चलता है कि दुर्घटना से ठीक पहले शिउली ने अपने सहपाठी डैन के बारे में पूछा था- ‘व्हेयर इज डैन? बस, यह बात डैन को मथ डालती है’ क्यों पूछा था…! वह सारे दोस्तों को खूब फटकारता है’ इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने मुझे बताई नहीं…!! सब उसे समझाते हैं। वह पूछना कुछ खास नहीं, बेहद सामान्य था। वह तुममें कोई वैसी रुचि नहीं रखती। लेकिन हादसे से पहले के इस वाक्य को डैन बहुत गंभीरता से लेता है- ‘अब मैं उसे कैसे जवाब दूं कि उस वक़्त मैं कहां था…?। और रोज अस्पताल जाने लगता है गोया जवाब देने के लिए ही। मित्र उससे पूछते हैं- तुम इतने प्रभावित कैसे हो गए? डैन का पलट जवाब- तुम लोग इतने अप्रभावित कैसे रह गए…? सबका कहना है- वो तो किसी को पहचानती भी नहीं। और डैन का उत्तर- तुम लोग तो उसे पहचानते हो…!
बस, डैन के इसी जज्बे की फिल्म है ‘अक्टोबर’। फिल्म का समाज है- डैन-सिउली के सारे सहपाठी और होटल के कर्मचारी व अफसर, जिनका इस जज्बे को न समझ पाना आज के समाज का इस जज्बे को न समझ पाने का प्रतीक है। और यही फिल्म की नोंक है, जिसे चुभाकर लुप्त होती संवेदना को छेड़ना चाहते हैं निर्देशक शूजित (अंग्रेजी वर्तनी का ठीक ठीक अनुवाद) सरकार और लेखिका जुही चतुर्वेदी। इस युति ने ‘विक्की डोनर’ में वीर्य-विक्रय जैसे विरल व धांसू एवं ‘पीकू’ में अपच (कॉंस्टिपेशन) जैसे अति सामान्य विषयों को जिस तरह सफलता पूर्वक बहुत खास बना दिया था, देखना है कि अब यह गहन संवेदनशीलता वैसे ही खास व ग्राह्य बनती है कि नहीं। संवेदन की यह लड़ाई नित संवेदनहीन होते जाते समाज के साथ है, जिसके लिए 45 सालों पहले दुष्यंतकुमार ने कहा था- ‘इस शहर में अब कोई बारात हो या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं हैं खिड़कियां…’ और उससे थोड़ा पहले सिद्ध कर चुके थे कमलेश्वर कहानी लिखकर ‘दिल्ली में एक मौत’, जिसमें शहर के सबसे बडेÞ आदमी की शवयात्रा में सिर्फ सात आदमी थे- सातवां लेखक ही था।
लेकिन यह समाज हमेशा ऐसा ही नहीं था। 1913 में अमृतसर की एक दुकान पर प्राय: दिख जाने पर लड़की से ‘तेरी कुड़माई (सगाई) हो गई’ पूछने वाले लहना ने उसकी कुड़माई व शादी हो जाने के बाद कभी शादी नहीं की और बहुत दिनों बाद उसके द्वारा अपने पति-बेटे की रक्षा करने की बात को पूरा करने में अपनी जान दे दी और उन दोनों से संदेश भेजा- ‘जाके उससे कहना कि मैंने वो किया, जो ‘उसने कहा था’। तब गुलेरीजी के लहना के उस जज्बे को समझा गया, जिसका प्रमाण है कहानी का क्लासिक हो जाना, लेकिन पहले सप्ताह के तीसरे दिन 4-5 सौ की सीटों वाले सिनेमाघर में ‘अक्टोबर’ देखने आए 20-25 लोगों से जाहिर है कि आज इस जज्बे को समझने वालों का कितना अभाव है और संवेदना की यह लड़ाई आज कितनी मुश्किल है…! लेकिन बकौल शूजित, उन्हें दर्शकता की परवाह नहीं। शायद तभी बना सके वे ऐसी फिल्म, जो आपको खींचती नहीं, मांग करती है कि आप उसकी तरफ खिंचें। अपनी बात बहुत धीमी गति से कहती है। शायद इतनी गहन बात तेज गति से कही ही नहीं जा सकती। और 20-25 मिनट में जब ‘रसे-रसे मन में समाय’ जाती है, तो ‘समइया बिलमे ना’ को यूँ सार्थक करती है कि निकलने के बाद मुंबई के ओपेरा हाउस जैसे भीड़-भरे इलाके एवं कवि मित्र देवमणि पांडेय के साथ होने के बावजूद बहुत देर तक कुछ भी बोलने की हालत नहीं रह जाती- एव्री गुड पोइट्री मेक्स मी सैड। और पूरी फिल्म ‘सैड’ क्या, त्रासदी का मानक है।
शिउली-डैन के इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया जा सकता, पर प्रेम के सिवा इसका कोई नाम हो भी नहीं सकता। लेकिन शूजित खुद कहते हैं और सही कहते हैं कि ‘यह प्रेम कथा नहीं, प्रेम की कथा है’, क्योंकि जिस तरह दर्शकों का यह समाज समझना नहीं चाह रहा इस जज्बे को, उसी तरह प्रेम कह देने से लोग नहीं समझेंगे कि यह प्रेम है। क्योंकि आज प्रेम का और फिल्म में प्रेम का मतलब है- ‘पहाड़ों-नदियों-समुद्रों, बाग-बागीचों-अमराइयों में उछल-उछल, नाच-गा-गा कर, हर दृश्य में दर्जन भर खुले-अधखुले रंग-बिरंगी पहनावे बदल-बदल कर आलिंगन-चुंबन करते हुए एक दूसरे पर गिरना-चिपकना और कहना- ईलू-ईलू…। ऐसे में यहां पूरे शरीर में ढेरों नलियों-पाइपों, पट्टियों-प्लास्टरों में बंधी, अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में पड़ी मृतप्राय लड़की को रोज देखने आने को लोग प्यार कैसे समझ सकते हैं! सो, यह लड़ाई समाज से ही नहीं, सिने-कला व सिने-संसार से भी है। प्यार की इस व्यवस्था-पने (सिस्टमाइजेशन) से भी है। बाह्य रंगीनियों पर लट्टू उपभोगवादी वृत्ति से भी है… यानी कई-कई गुत्थियां सुलझानी हैं, बाड़ें तोड़नी हैं। इसी से प्रेम की कथा है, कहकर गोया नए सिरे से परिभाषित करना पड़ता है कि यह भी प्यार है या प्यार यह है…। यहां कोमा में पड़ी उस किशोरवय नायिका शिउली (वनिता सन्धू) से 21 साला नायक दानिश उर्फ डैन (वरुण धवन) बात करता है। यह जीवन विहीन चेतनता से जीवन का संवाद है…।
इसमें मानस व हृदय के कई मोड़ व कोण बनते हैं। मूत्र ज्यादा आया, क्या कल ज्यादा पानी पिला दिया था, के निरीक्षण और सोच से हरसिंगार के फूल लाकर सिरहाने रख देने तक की यात्रा में अपने संपूर्ण प्रयत्न को वार देता है डैन…। बंगला शब्द शिउली का अर्थ ही है हरसिंगार। यह संगति कलात्मक है। असर होता है। शिउली तक अपनी बात पहुंचाने के लिए डैन अपनी संपूर्ण चेतना को झोंक देता है। डॉ. घोष (आशीष घोष) को अपने मेडिकल प्रयत्नों का असर लगता है। अंग-संचालन के बाद पहला संवाद आँखों से होता है। सुन्दर हैं वनिता सन्धू की आँखें। डॉ. के आदेश पर पुतलियां बाएं-दाएं घूमती हैं- ‘माँ की तरफ, पर डैन की तरफ नहीं घूमतीं’ ‘नैंन की बात है नैंन ही जानें’…। पर नहीं, शिउली के मन की बात है- डैन ही जाने…। एकांत में दुलराता है- ‘अच्छा किया सबके सामने मुझे नहीं पहचाना…। और अकेले में डैन के कहने पर आँखें उसकी तरफ घूमती हैं… निहाल हो उठता है डैन और गहरे मुतासिर हो उठते हैं हम…। संवाद की ऐसी आकुलता खोज ही लेती है सम्प्रेषण की राह। तन के रहते प्राण की बात प्राण तक पहुँचती है। यह ‘मिल सकें ना प्राण प्राणों से, दीवार है तन’ वाली कवि की अध्यात्म की बात से आगे की बात है। साकार होती है अंतर्मन की सचाई पर्दे पर…। यही है फिल्म।
पर सवाल होगा- जब आज नहीं है कहीं, तो यह जज्बा डैन में कहाँ से आया…? इसी को साधते हुए फिल्मकार ने डैन को दुनिया से थोड़ा अलग बनाया है- बेबाक व बेपरवाह। जिन बातों को बाकी छात्र सह लेते हैं, वह झल्ला कर बोल देता है- 202 नम्बर के बंडल में अंडरवेयर किसने प्रेस कर दी? पता है एलास्टिक ढीला हो जाता है…! सर, मैं हमेशा मक्खी-मच्छर मारने के लिए तो नहीं आया हूँ न…। और एक ग्राहक (कस्टमर) की बेजा बोलबाजी पर पेशेवर संहिता को तोड़ते हुए उसके साथ की औरत के सामने ही कह देता है- पिछली बार आप शायद अपनी पूर्व पत्नी (एक्स वाइफ) के साथ आए थे। … ये हरकतें उसके विरल (रेयर) और खास तथा गैर दुनियादार बताने के लिए उसके चरित्र-विकास की सगतियों के लिए ही गूँथी गई हैं। इस स्वभाव को वह भी जानता है, इसी से नौकरी न करके अपना होटेल खोलना चाहता है। इन अनियमितताओं के लिए उसे बार-बार चेतावनियां दी जाती हैं, पर उसकी ढिठाई जाती नहीं। तभी तो आगे चलकर शिउली के लिए रोज अस्पताल जाने में नियमित काम नहीं कर पाने की परवाह नहीं करना समझ में आता है। लेकिन शिउली की तरफ उसकी संसक्ति बढ़ती जाती है और उसमें सुधार न होने से खिन्नता भी…, जिसके चलते एक दिन खाना देते हुए एक शख़्स की बदमजगी पर उसे बुरी तरह पीट देता है और निकाल दिया जाता है…।
तीन लाख का जुर्माना भरने आती है डैन की माँ, तो पता लगता है कि दस महीने से उसने घर एक फोन भी नहीं किया है… ऐसा है जज्बा, तब खुलता है चेतना से चेतना तक पहुँचने का राजमार्ग। पर तभी फिल्म यह भी दिखा पाती है कि दुनिया समझे, न समझे, अस्पताल जाकर सब कुछ जान-देख लेने पर डैन की माँ समझ पाती है। उसी से बताते हुए शिउली की माँ भी डैन के जज्बे को रेखांकित करती है कि शिउली के जीवन-पथ्य का आधार-स्तम्भ है डैन की भूमिका…। होटल प्रबन्धन की दुनिया भले न समझे, अस्पताल की दुनिया ने डैन को समझा और अपना लिया है- अब नर्स उसके प्रश्नों से झल्लाकर भगाती नहीं, खुद उत्तर देने के लिए बुलाती है। और दर्शक देखता है कि डैन की यह देख-भाल करने की सांसारिक भूमिका नहीं, वरन बेहद विरल रूप से संवेदनात्मक सम्बल की भूमिका है। तभी तो एक बार डैन के नौकरी करने चले जाने पर शिउली बेकाबू (वाइल्ड) हो जाती है, तो फिर आकर डैन प्रतिज्ञा करता है कि अब कभी नहीं जाएगा। और उसके मरने तक नहीं जाता…।
फिल्म आद्यंत त्रासदी पूरी फिल्म के दौरान विद्या अय्यर नाम से माँ बनी गीतांजले राव के चेहरे पर खुदी हुई पढ़ी जा सकती है। और शिउली का होना डैन के चेहरे पर हरसिंगार-सा झरता रहता है। मैंने भी वरुण धवन की कोई फिल्म नहीं देखी थी- जैसे बकौल शूजित, उन्होंने भी नहीं देखी थी, पर एक बार देखकर भूमिका के लायक समझ लिया और हमने देखकर उसे डैन ही समझा। जाने कैसे करता होगा वह चॉकलेटी और चालू भूमिकाएं…। लगभग पूरी फिल्म मृत्यु-शय्या पर पड़ी वनिता सन्धू शरीर रहते अशरीरी होकर जीवन की प्रेरणा बन जाती है। कभी कैंसर के मरीज बनकर एक खाट पर बैठे-लेटे राजकुमार के जलवे हमने ‘दिल एक मन्दिर’ में देखे थे और उनके सितारेपन (स्टारडम) के मुरीद हुए थे, पर वनिता ने ऐसा मुतासिर किया कि उस जलवे की स्मृति दिखावटी लगने लगी है। लेकिन ये सब सृष्टि तो हैं जुही चतुर्वेदी की, जिनने फिल्म नहीं, प्रेम की सूक्ष्मता का त्रासद महाकाव्य रचा है और उसे उसी फलक से शूजित ने साँचा-दर साँचा रूपायित किया है, जिसे छायांकन में अविक मुखोपाध्याय ने अदद रूप से जीवंत किया है और शांतनु मोइत्रा का संगीत ‘भीतर हाथ सहारि दै’ की अर्थवत्ता है।
अक्टूबर का महीना हरसिंगार के खिलने के मौसम के रूप में जाना जाता है, पर इन सबसे सृजित यह ‘अक्टोबर’ बारहमासी बन पड़ी है। और चेतनता से संवाद की ऐसी रीलें रुकती कहाँ हैं- मन से मन तक में उपराम पाती रहती हैं अनवरत…।