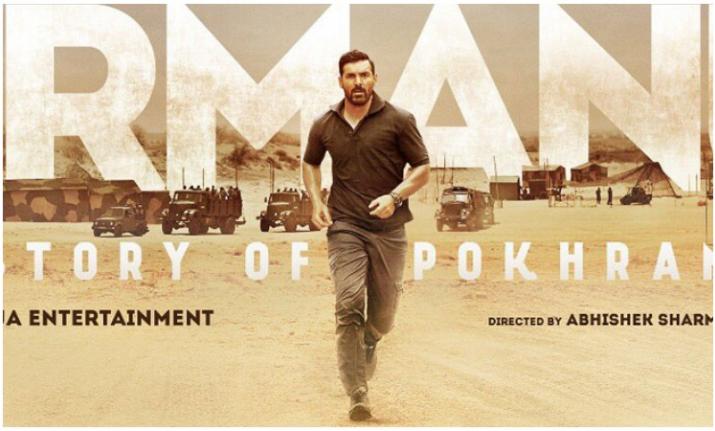सत्यदेव त्रिपाठी
-मैं अपनी कहानियों को एक आईना समझता हूं, जिसमें समाज अपने को देख सके।
-और यदि सूरत ही बुरी हो, तो आईने का क्या…?
-मैं सोसाइटी के चोले क्या उतारूंगा, जो पहले से ही नंगी है!
-यदि आप मेरी कहानियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो यह जमाना ही नाकाबिलेबर्दाश्त है… आदि-आदि।
ये तेवर हैं फिल्म ‘मंटो’ में’ उर्दू के सरनाम अफसानानिगार सआदत हसन मंटो साहब के, जिसे बर्दाश्त न कर सके पिछली सदी के चौथे-पांचवें दशक के मर्द, मजहबी, हुक़्मरान और फनकार व अदीब भी- उसी दौर के प्रगतिशील शायर फैज तक ने ‘ठंडा गोश्त’ के ताल्लुक से मंटो की कहानियों को फाहिश (अश्लील) न सही, साहित्य के दर्जे का नहीं माना। यानी मंटो का पूरा समय उसे सह न सका। लिहाजा मंटो की कहानियों के आईने ही उसकी मरणांतक त्रासदी के सबब बने। तो क्या आज मंटो पर जीवनीपरक फिल्म बनाकर नन्दिता दास यही तो नहीं पूछना चाह रहीं कि ऐसे तेवर को क्या बर्दाश्त कर सकेगा आज का समाज, सत्ता, साहित्य और कला- यानी वही, आज का समय?
लेकिन इससे बड़ा सवाल यह कि क्या ऐसा तेवर आज बचा है लेखकों में? क्योंकि वे सच तो वैसे ही हैं, बल्कि आज कई गुना बढ़ गए हैं। बड़े होकर जीवन को झिंझोड़ भी रहे और झुलसा भी रहे हैं। जबकि आज जंग-ए-आजादी जैसी नृशंसता एवं मुल्क के बंटवारे जैसी वीभत्सता का कोई ऐतिहासिक हादसा भी नहीं है। तो क्या मंटो का इतनी मरणांतक पीड़ा सहकर भी तीखे तेवर को बनाए रखने के जरिये नन्दिताजी आज के लेखकों को तो नहीं ललकार रही हैं? जी हां, यही है इस फिल्म का सबब। खराद पर हैं इसमें आज के सच और उसके मुकाबिल सत्ता भी, समाज भी और रचनाकार भी। यही है फिल्म ‘मंटो’ के मौजूं होने की धनक। फिल्म की संरचना इतनी सांकेतिक है कि 71 साल पहले के समय को आज से जोड़ने वाले सूत्र फिल्म के परिवेश में भी टंके मिलते हैं- पुरानी शैली की इमारतें- पत्थर और खपरैल की बनी भी, पुराने काट के कपड़े, मुंबई की लोकल, आज भी कहीं-कहीं दिख जाती घोड़ा गाड़ियां, पारसी-ईरानी होटेल्स, तब के बागीचे…आदि।
कहानियों के आईने में नुमायां उन सचों की चर्चा पर आने से पहले दो बातें और… पहली यह कि काश, यह ललकार ‘संजू’ के हीरानी (हीरा+नी) भी सुनते और समझ पाते ‘बायोपिक’ का सही मतलब और मकसद! दूसरी यह कि जीवनी पर बनी फिल्म कल्पना से बनी कथा (फिक्शन) नहीं, किसी जीवन का सच होती है, इसलिए कौन सी घटना या चरित्र कैसा और क्यों हो गया या वह कैसा होता, तो क्या सरोकार बनते, की समीक्षा यहां बेमानी होती है। फिर जब 5-6 सालों से फिदाई की तरह इस फिल्म की पटकथा में डूबी नन्दिताजी जैसी प्रतिबद्ध व जहीन फिल्मकार के बर-अक्स तो ‘मंटो’ में उकेरी सआदत हसन संबंधी घटनाओं पर शक की गुंजाइश ही नहीं बनती- ये हौसला मुझको तेरे ‘कामों’ ने दिया है। बतौर उदाहरण मुंबई के प्रेम में आकंठ डूबे मंटो ने महज अपने गहरे हिन्दू मित्र की टिप्पणी के नाते पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया, जो उनकी जिन्दगी के बर्बाद होने की प्रमुख वजह बना और फिल्म तथा मंटो की जिन्दगी का निर्णायक मोड़ भी; तो इतनी-सी बात पर जीवन भर का संत्रास ले लेने के लिए फिल्म ‘मंटो’ या निर्देशिका पर शंका नहीं, इसे सआदत हसन की शख़्सियत का खुलासा समझना होगा। मित्र की भूमिका में श्याम बने ताहिर राज भसीन ने ‘मर्दानी’ में जो छाप छोड़ी, वह यहां छूटी नहीं। इसी तरह फिल्म का हर टुकड़ा मंटो के सोच व जिन्दगी के पट खोलता सिद्ध हुआ है और सिर्फ चार सालों (1946 से 50) पर आधारित यह बायोपिक मंटो ही नहीं, आज तक के भारत-पाकिस्तान के सफर के लिए भी कितनी अहम साबित हुई है, क्या बताने की जरूरत है?
यूं तो फिल्म जगत में हमेशा ही कोई न कोई चलन (ट्रेंड) चलता रहता है और आजकल जीवनीपरक (बॉयोपिक) फिल्में चलन में हैं, जिसमें सबसे हिट है खेल और खिलाड़ियों का जीवन, जिनकी उपलब्धियां अधिकांशत: बाह्य होती हैं, साफ दिखती हैं- उनके श्रम में व उनकी सफलता में। लेकिन किसी लेखक-कवि पर फिल्म बनाना बहुत जटिल काम है, क्योंकि उनका जीवन जितना और जैसा बाहर से दिखता है, उससे कहीं अधिक अंतस में पैठा रहता है, जिसके लिए मुहावरा बन गई है बच्चनजी की पंक्ति- ‘कवि का पंथ अनंत सर्प-सा, बाहर-भीतर पूंछ छिपाए’। और इसी जटिलता को साधने, मंटो के अंदरूनी पक्ष को खोलने की चुनौती के तोड़ के तहत नन्दिता ने उस काल के ज्वलंत इतिहास के साथ मंटो की रचनाओं-खासकर पांच कहानियों- को भी जोड़ लिया है, जो फिल्मकार का ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है। और ब्रह्मास्त्र की खासियत होती है- सब पर जीत की गारंटी और सबसे अकेला कर देना। तो यह रूपक यूं सही उतरता है फिल्म पर कि मंटो का अच्छा पाठक तो इस सिने-प्रक्रिया को, मंटो की जहनियत को समझेगा और फिल्म का भरपूर लुत्फ उठाएगा, पर आम दर्शक से दूर हो जाएगी फिल्म। और इस रूप में फिल्म एक खास समुदाय (क्लास) के लिए हो गई है। नतीजा दिखा भी- बहुत कम सिनेमाघरों में लग नाई। कई छोटे शहरों में लगी ही नहीं- पूछताछ होती रही। वितरकों के हवाले से इसी आशय की टिप्पणी की नन्दिता ने भी। और मुंबई जैसे विराट नगर में जिन थोड़ी-सी जगहों पर लगी भी, उनमें पहले दिन (डे वन) से ही आलम यह रहा कि तीन-साढ़े तीन सौ लोगों की क्षमता वाले ‘जेमिनी’ (बान्द्रा-पश्चिम) में बमुश्किल 50-60 दर्शक थे। इस मुद्दे पर कहना होगा कि दर्शक से भी थोड़ी-सी तैयारी (होम वर्क) की मांग करती है फिल्म- कम से कम इतनी कि निर्देशिका ने पांच साल तैयारी की, तो दर्शक पांच कहानियां तो पढ़ें। और उन 50-60 में 10-12 का एक समूह था, जो जानकार था और मंटो के संवादों व अन्य पुरजोर अवसरों का लुत्फ ले ही नहीं रहा था, टिप्पणियों, कहकहों और तालियों आदि से सबके लिए लुत्फ लुटा भी रहा था।
अब आइए, समय और हालात के साथ कहानियों को जोड़ने की प्रक्रिया का जायजा लें। दो खास सच हैं मंटो के लेखन में- स्त्री का तमामों रूपों में दैहिक शोषण और बंटवारे की मर्मांतक पीड़ा। यही दोनों सच मंटो को मंटो बनाते हैं। इतने रूप और चेहरे हैं इसके मंटोनामे में कि क्या कहने… और एक से एक तंज लिए हुए तेज से तेजतर। फिल्म में दो कहानियां खांटी तौर से स्त्री पर हैं। शुरुआत ‘दस रुपये’ से होती है, जिसमें किशोरी लड़की को वेश्या के रूप में ढाल दिया है घर वालों ने ही। और वह कार में ग्राहकों के साथ जाती है, समुद्र-तट पर पानी में खेलती है। खेलने की उम्र में खेल का यह विद्रूप! फिर ‘सौ वॉट का बल्व’ में शायद पति है, पर औरतों का दलाल (परेश रावल) है। चौराहे पर ग्राहक को पटाने में जितना विनम्र और दयनीय, कमरे में जाकर उतना ही पेशेवर। सोने-खाने का समय भी नहीं देता उस बेजान-सी काया को। अपनी बेबसी बताने पर खुशामद और संवेदना से मनाता है, पर न मानने पर उस मरेली-सी को मारपीट कर भी धंधे के लिए भेजने में शातिर। इतना ही है फिल्म में- यह सवाल उठाता हुआ कि उसी धंधे से खाने वाला यह मुस्टंडा खुद क्या करता है? इस तरह स्त्री के दो मुख्य पालक व पवित्र रिश्तों वाली कहानियों को चुनकर नन्दिताजी ने मंटो के सोच का एक मुकम्मल आईना रखा है। शेष तीनों कहानियां बहुत-बहुत मशहूर हैं, जिनमें अगली दो कहानियों ‘खोल दो’ व ‘ठंडा गोश्त’ में बंटवारे के काफिरेपन में स्त्री की शर्मनाक त्रासदी है। ‘ठंडा गोश्त’ सर्वाधिक कुख्यात हुई। यही फिल्म का चरम (क्लाइमेक्स) है। पाकिस्तान में इसी पर मुकदमा चलता है, जहां अदीब भी बेपर्द होते हैं। मरहूम फैज की अदबी छबि उघड़ती है, तो आबिद अली आबिद बने चिरंजीव जावेद अख़्तर अपने अदा-ओ-अन्दाज में ठस्स होकर रह जाते हैं। फिल्म वहीं मंटो के कहे को मंटो बने नवाजुद्दीन से कहलवा कर अपने कला-कर्म को अंजाम देती है कि ऐसा करने वाला पूरा समाज (पति व मां-बाप तक) आजाद है, पर इस घृणित सच को आईना दिखाने वाले लेखक पर केस चलता है।
इस चरम के बाद अंत होता है विभाजन की खांटी कहानी से। फिल्म के लिए सबसे धारदार व कई-कई मर्म भरे संकेतों से युक्त संयोजन में फिल्म-रूपायन की कला पाती है अपनी चरमरति (और्गाज्म) के क्षण। विभाजन में देश ही नहीं बंटा दो भागों में, वरन मंटो का जीवन जहां गुजरा, जहां दोस्त-यार रहे, जहां अफसानों के साथ हिन्दी फिल्मों आदि के लिए भी कहानियां लिखते हुए नाम-दाम पाया… और जहां मां-पिता व बेटा भी दफ्न रहे, ऐसी बहुत-बहुत प्यारी, अजीज और दिलकश अपनी बम्बई (अब मुंबई)…जिसके छूटने और लाहौर जाकर ठौर पाने में मंटो भी दो भागों में बंट गया था। और इस मुकाम पर आकर उसी का आईना बनते हुए फिल्म भी दो भागों में बंट गई है। फिर ऐसा कैसे संभव है कि बनाने वाली साबुत रह गई हो? फिर फांक होने से कैसे बच सकेगा कोई जहीन दर्शक भी? अंतिम हिस्से तक जाते-जाते इस फांक का आईना तब फिल्म के आदमकद हो जाता है, जब कहानी ‘टोबा टेक सिंह’ का संदर्भ जुड़ता है। देश के बंटवारे के बाद किसी आम आदमी की समझ में यह कानून नहीं आया और उसका पालन कराने वाले फौजियों का सलूक समझ में नहीं आया कि कल तक जो घर सात पुस्तों से अपना था, जो पड़ोसी सदियों से दुख-सुख के साथी थे, वह घर पराया और पड़ोसी अजनबी कैसे हो सकते हैं। इसी आम आदमी का प्रतिनिधि है वह सरदार टोबाटेक सिंह। मरता है दोनों देशों की सरहद पर- किसी की जमीन में नहीं (नो मैन्स लैंड में)। पर मरता कौन है? क्या सिर्फ सरदार? या सिर्फ मंटो का प्रतिनिधि सरदार? महाभारत के कृष्ण ने ‘अन्धायुग’ में कहा है- हर सैनिक के साथ मैं ही तो मरा हूं…। लेकिन यहां कोई कृष्ण नहीं है- सबके देश तय हो गए थे। सो, मरते हैं दो देश! लेकिन इतने तीखे-कसैले-कड़वे सचों को पालते-पालते और उनसे उबल-उबल कर उफनते-उफनते मंटो बार-बार मर चुका था- जब-जब दुनिया ने इसके आईने में छवि अपनी देखी और पत्थर मंटो को मारे… जब संपादक ने उसका कॉलम लौटाया, तो पन्ने फाड़कर उसके मुंह पर फेंकते हुए मंटो ही तो मरा… दोस्त के मुंह से अचानक ही सही, ताना सुनकर ‘इतना मुसलमान तो हूं ही कि मारा जाऊं…’ कहते हुए… ‘ठंडा गोश्त’ के पन्ने वापस लेकर सीढ़ियां उतरते हुए… कोर्ट में लोगों के आरोप सुनते हुए… और बेहद आजिजी से अपनी तकरीर करते हुए… और सबके बाद दवा तक के लिए बेबस होते हुए- लेकिन सबसे त्रासद मौत तब हुई होगी, जब पत्नी सफिया से सुनना हुआ- तुम्हारे लिखने के कारण ही हम मरेंगे, लेकिन यह कहते हुए इतनी उदार-शालीन-सहयोगी सफिया भी जिंदा कहां रही होगी? इन रूपों को अत्यंत संयम व सलीके से साकार करती सुरूपवती रसिका दुग्गल दर्शनीय ही नहीं, चिरकाल तक स्मरणीय रहेंगी। लेकिन गरज ये कि सच का आईना दिखाने में मंटो ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई।
फिल्म की अतल गहराई से रिसती है यह बात भी कि मंटो ने भी सिर्फ आईना ही दिखाया। स्त्री-बेचकों को आईना दिखाया, संपादक के मुंह पर पन्ने दे मारे, पर जब बड़ा फिल्म-निर्माता (ऋषि कपूर) किसी औरत की जिस्म-नुमाई कर रहा था, तो देखकर भी अनदेखा करते हुए जो लौट आया, वो मंटो ही था। सारे असह्य को सहने के लिए पानी से भी ज्यादा शराब में डूबा, सिगरेट में फूंका, पर कुछ करने की पहलकदमी नहीं की। बख़्शती नहीं फिल्म इस लत तक को। बच्ची से कहलवा ही देती है- तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही…। यानी फिल्मकार की ‘नजरे-इनायत’ से बचता कोई नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन इतना सब करते हुए कुछ शेष नहीं छोड़ते नवाजुद्दीन भी… और मजा यह कि किसी दृश्य में नि:शेष होते भी नहीं दिखते- अभिव्यक्ति की भूख और सम्प्रेषण ऊर्जा का कोष इतना अजस्र है कि कितना भी उड़ेलो, भरा-भरा ही रहता है। शुरू में सुनगुन थी कि इरफान करेंगे यह भूमिका, पर नवाजुद्दीन को देखकर लगा कि इसी के लिए बने हैं वे- वे ही बने थे इसके लिए। बताया भी नवाज ने कि मंटो जैसा चलना-बोलना-दिखना तो आसान है, पर उनकी विचार-चेतना (थॉट प्रोसेस) तक पहुंचना, उसे पाना आसान न था… मुहय्या कराया नन्दिता दास ने और इनके बनाए माहौल ने। दास ने जो विधान रचा, उसमें मंटो के आईने का रूपक यूं फला-फूला कि सारे संवाद सांग रूपक (कंपाउंड मेटॉफर) बन जाते हैं। फूहड़-से दृश्यों में कला का सौन्दर्य झांकने लगता है और जो माहौल बना मंटो के मुंबई-जीवन का, उसमें इस्मत चुगताई (राजश्री देशपांडे), जद्दन बाई (इला अरुण), नरगिस (फरयाना वजैर), अशोक कुमार (भानु उदय) आदि के मेले ने जो सतरंगी पृष्ठभूमि रची, उस पर आगे चलकर लाहौर का जो चिलचिलाता माहौल बरपा हुआ, वह खिला भले न हो विरोधाभास (कंट्रास्ट) में खुला है अवश्य खूब। यह सब सृजित करने में नन्दिताजी तो ‘तरे, जे बूडेÞ सब अंग’ हो गई हैं। और इतना डूबने पर अभिव्यक्ति का जो परम सुख मिलता है, उसमें कहां ख्याल रह जाता है कि कौन देखेगा… सो कोई समझौता नहीं। लेकिन वही संजीदा डूबना ही है कि पूरी फिल्म में कसकती-कराहती अभिव्यक्ति की त्रासदी से टकरा पाता है, उसे व्यक्त कर पाता है, उसे गहरा पाता है… ‘डूबकर हो जाओगे पार’ को सार्थक कर पाता है।
फिल्म के गीत ‘अब क्या बताऊं हाल (शुभा जोशी), नगरी-नगरी (स्नेहा खानवेलकर) आदि सबकुछ को महकाते भले न हों, भीने-भीने भिगाते जरूर हैं। नन्दिताजी ने भले फिल्म का अंत किया हो ‘बोल कि लब आजाद हैं तेरे’ से- न जाने क्यों- फैज के किंचित स्याह नजरिये को दिखाने के बावजूद… पर मैं तो लेख को संपन्न करूंगा मंटो के सच के आईने के मुतालिक इस कथन से- ‘नीम के पत्ते कड़वे भले होते हों, खून तो साफ करते हैं!