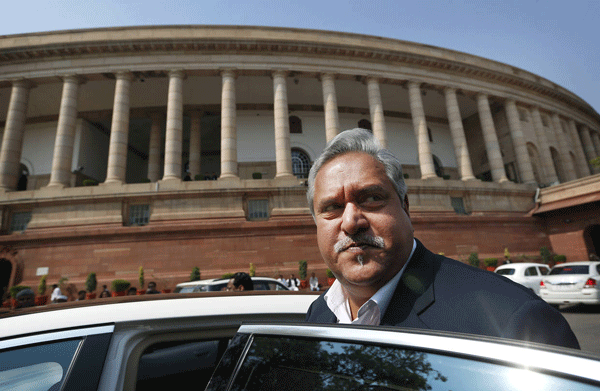आनंद प्रधान
कहना मुश्किल है कि ‘अच्छे दिनों के महाराजा’ समय के फेर में फंस गए हैं या उनके चमकते सितारे खराब हैं या फिर अपनी पांच सितारा पार्टियों के लिए मशहूर उद्योगपति विजय माल्या ने खुद मुसीबत को दावत दी है। कारण चाहे जो हो लेकिन अपनी तड़क-भड़क भरी जीवनशैली और शाहखर्ची के लिए अकसर सुर्खियों में रहने वाले माल्या इन दिनों सरकारी बैंकों से कर्ज के तौर पर लिए 7,200 करोड़ रुपये को जानबूझ कर नहीं चुकाने (विलफुल डिफॉल्टर) या डकारने के कारण सुर्खियों में हैं। न्यूज चैनल, अखबार और सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता अचानक सक्रिय हो गए हैं और माल्या की गिरफ्तारी से लेकर बैंकों का बकाया वसूलने की मुहिम का शोर तेज हो गया है।
हैरानी की बात यह है कि सरकारी बैंकों के हजारों करोड़ रुपये डकारने के आरोप विजय माल्या पर पिछले कई साल से लग रहे हैं। उनकी एयरलाइन किंगफिशर को बंद हुए तीन साल से अधिक हो गए हैं और इसके साथ ही उसमें लगे सरकारी बैंकों के हजारों करोड़ रुपये भी फंस गए। यह भी किसी से छुपा नहीं है कि किंगफिशर एयरलाइन माल्या के मनमाने फैसलों, शाहखर्ची और कुप्रबंधन के कारण डूबी। इस तथ्य को जानते हुए भी कि एयरलाइन की वित्तीय हालत खराब है और उसकी सबसे बड़ी वजह माल्या खुद हैं, सरकारी बैंकों ने किंगफिशर पर बहुत बाद तक पैसा लुटाना जारी रखा। यहां तक कि बैंकों ने सैकड़ों करोड़ रुपये का कर्ज देते हुए कोई संपत्ति गिरवी/बंधक (कोलेटरल) नहीं रखी। मजे की बात यह है कि कुछ बैंकों ने तो किंगफिशर (ब्रांड) नाम को ही कोलेटरल मानकर कर्ज दे दिया।
हजारों करोड़ रुपये डकार कर सरकारी बैंकों को चूना लगाने वाले विजय माल्या अकेले उद्योगपति नहीं हैं। ऐसे दर्जनों उद्योगपति और कॉरपोरेट समूह हैं जिन्होंने सरकारी बैंकों से माल्या से भी ज्यादा उधार ले रखा है
किंगफिशर एयरलाइन डूब गई, उसमें बैंकों के हजारों करोड़ रुपये फंस गए, उसके अधिकारियों/कर्मचारियों का महीनों का वेतन और दूसरे बकाये फंस गए लेकिन विजय माल्या की पांच सितारा जीवनशैली में कोई बदलाव नहीं आया। उनके दूसरे कारोबार/धंधे जारी रहे। माल्या ने अपनी मूल शराब कंपनी यूनाइटेड बे्रवरीज को विदेशी शराब कंपनी डियाजियो को बेच दिया। कहने को तो कई सरकारी एजेंसियां जांच करती रहीं और बैंक अपना पैसा वसूलने के लिए दिखावा भी करते रहे। वे बतौर राज्यसभा सांसद कभी-कभार संसद भी आते रहे। माल्या के राजनीतिक रसूख और कॉरपोरेट ताकत का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसी साल फरवरी के आखिरी सप्ताह में जब सरकारी बैंकों के बढ़ते खराब कर्ज यानी एनपीए के सिलसिले में सरकार और बैंकों पर माल्या से पैसा वसूलने और गिरफ्तारी का दबाव बढ़ने लगा तो वे चुपके से देश से निकल गए।
क्या माल्या अगले ललित मोदी साबित होंगे? कहना मुश्किल है लेकिन दोनों ही मामलों में राजनीतिक रसूख और कॉरपोरेट ताकत के जरिये नियम, कानून और जांच को ठेंगा दिखाने का दुस्साहस लगभग एक जैसा है। हालांकि माल्या कथा अभी खत्म नहीं हुई है लेकिन इस पूरे प्रकरण में पिछली यूपीए और मौजूदा एनडीए सरकार के रवैये पर दर्जनों सवाल खड़े होते हैं। माल्या का इस तरह से देश से निकल जाना इस बात का सबूत है कि नियम-कानून ताकतवर लोगों पर उसी तरह लागू नहीं होते हैं जैसे गरीबों और आम लोगों पर लागू होते हैं। दोहराने की जरूरत नहीं है कि बैंक से कुछ हजार रुपये का कर्ज लेने वाले एक गरीब किसान को फसल खराब होने के बाद कर्ज न चुका पाने की स्थिति में किस तरह से जेल भेजने और कुर्की से लेकर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है और उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है।
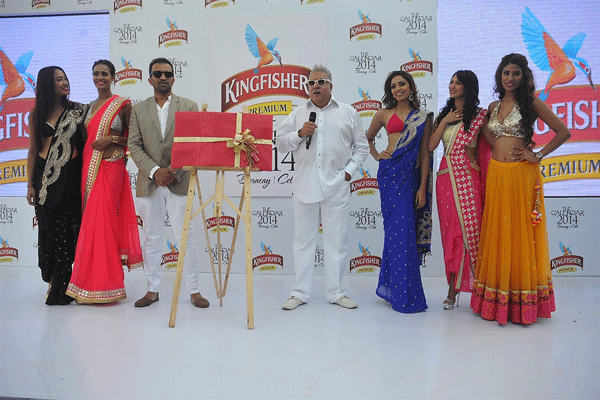
यह सच है कि हजारों करोड़ रुपये डकार कर सरकारी बैंकों को चूना लगाने वाले विजय माल्या अकेले उद्योगपति नहीं हैं। तथ्य यह है कि अपने राजनीतिक संबंधों और प्रभाव के लिए मशहूर ऐसे दर्जनों उद्योगपति और कॉरपोरेट समूह हैं जिन्होंने सरकारी बैंकों से माल्या से भी ज्यादा उधार ले रखा है जिसका बड़ा हिस्सा डूब चुका है या डूबने की कगार पर है। इसके बावजूद माल्या अगर बैंकों का कर्ज डकारने वाले ताकतवर कॉरपोरेट के ‘पोस्टर बॉय’ बन गए हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह वे खुद हैं। असल में माल्या सरकारी बैंकों के पैसे और प्राकृतिक संसाधनों की लूट पर फलने-फूलने वाले याराना पूंजीवाद (क्रोनी कैपिटलिज्म) के ऐसे प्रतीक बन गए हैं जो न सिर्फ अपनी राजनीतिक पहुंच, प्रभाव और पैसे की ताकत से सभी नियम-कानूनों को धता बताते हुए अपना साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब होते हैं बल्कि उनकी मनमानियों और तुगलकी फैसलों, फिजूलखर्ची और कुप्रबंधन का खामियाजा भी सीधे या परोक्ष रूप से आम लोगों को चुकाना पड़ता है।
माल्या जैसे याराना पूंजीवाद की पैदाइश कई हैं। माल्या पर शुरू हुए शोर-शराबे की अच्छी बात यह है कि उनके सुर्खियों में आने और कुछ न्यूज चैनलों के अभियान के कारण राजनीतिक तंत्र पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा है। यह जरूरी है क्योंकि माल्या पर सख्ती और कार्रवाई से दूसरे कॉरपोरेट डिफॉल्टरों और बैंकों का पैसा डकारने वालों खासकर जानबूझ कर कर्ज न चुकाने वाले (विलफुल डिफॉल्टरों) को एक कड़ा संदेश जाएगा। लेकिन माल्या पर अत्यधिक फोकस के नुकसान भी हैं। इससे एक तो ऐसा लगता है कि जैसे यह समस्या सिर्फ विजय माल्या तक सीमित है, दूसरा, इससे असल मुद्दे यानी सरकारी बैंकों के पैसे की लूट का मसला पृष्ठभूमि में चला गया है। इससे कई बड़े कॉरपोरेट अपराधियों और उनके राजनीतिक और बैंकों के प्रबंधन से जुड़े संरक्षणकतार्ओं को बचकर निकलने का मौका मिलता दिख रहा है।
बैंकों का बढ़ता एनपीए : वित्तीय व्यवस्था के लिए खतरा
असल में मुद्दा यह है कि पिछले तीन-चार सालों में सरकारी बैंकों के एनपीए यानी डूबा कर्ज और उसे बट्टा खाते में डालने में खतरनाक रूप से वृद्धि हुई है। इन बैकों का लाखों करोड़ रुपये का कर्ज डूब गया है या डूबने की कगार पर है। कहने की जरूरत नहीं है कि यह पैसा बैंकों में अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा जमा करने वाले आम लोगों का है। इससे न सिर्फ आम लोगों की बचत खतरे में है बल्कि इसके कारण बैंक नया कर्ज नहीं दे पा रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में नए पूंजी निवेश पर ब्रेक लग गया है और बैंकों की साख पर भी असर पड़ा है। इससे पूरी वित्तीय व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया है क्योंकि बैंक वित्तीय व्यवस्था के मुख्य आधार हैं। याद रहे कि अमेरिकी बैंकों के डूबने के कारण ही 2008 में वैश्विक अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ गई थी और वह अपने साथ आर्थिक मंदी लेकर आई थी जिससे दुनिया आज भी जूझ रही है।
माल्या पर शुरू हुए शोर-शराबे की अच्छी बात यह है कि राजनीतिक तंत्र पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा है। यह जरूरी है क्योंकि माल्या पर सख्ती और कार्रवाई से दूसरे कॉरपोरेट डिफॉल्टरों को एक कड़ा संदेश जाएगा
सरकारी बैंकों के खराब कर्ज (बैड लोन) और डूबते कर्ज (एनपीए) के कारण उसे बिगड़ती स्थिति से उबारने के लिए केंद्र सरकार को सरकारी खजाने से भरपाई करनी पड़ रही है। वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 25 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हालांकि बैंकों के डूबे हुए कर्ज की तुलना में यह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है लेकिन यह रकम भी आम लोगों के टैक्स का पैसा है जो किसी और बेहतर काम में खर्च हो सकता था। यह याराना पूंजीवाद के मूल सिद्धांत ‘मुनाफे का निजीकरण और घाटे का सरकारीकरण’ का एक और उदाहरण है।
सरकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति कितनी खराब है, इसका अंदाजा ‘इंडियन एक्सप्रेस’ अखबार की इस रिपोर्ट से लगाया जा सकता है कि वित्त वर्ष 2013-15 में सरकारी क्षेत्र के 29 वाणिज्यिक बैंकों ने 1.14 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को खराब कर्ज (बैड लोन) बताकर बट्टे खाते में डाल दिया। यह मामूली रकम नहीं है। वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के कुल बजट से यह ज्यादा है। यही नहीं, सरकारी बैंकों का एनपीए किस तेजी से बढ़ रहा है इसका अनुमान वित्त मंत्री अरुण जेटली के राज्यसभा में दिए इस उत्तर से लगाया जा सकता है कि सरकारी बैंकों का एनपीए वित्त वर्ष 2015-16 में अप्रैल से दिसंबर के नौ महीनों में 94,666 करोड़ रुपये बढ़ गया। इस तरह सरकारी बैंकों का एनपीए जो मार्च 2015 में 2,67,065 करोड़ रुपये था, वह दिसंबर 15 में बढ़कर 3,61,731 करोड़ रुपये हो गया है।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिसंबर 15 तक सरकारी बैंकों के कुल एनपीए में से 1,30,156 करोड़ रुपये उन बड़े कर्जदारों का है जिन्होंने 500 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया है। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के मुताबिक, 30 सबसे बड़े कर्जदारों के कुल कर्ज और एक करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लेने वालों का अनुपात 51.79 फीसदी है। इसी तरह एनपीए को बट्टे खाते में डालने के बाद बैंकों की ओर से कर्जदार की संपत्तियां बेचकर पैसा वसूलने में भी गिरावट आई है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, रिकवरी की जो दर वित्त वर्ष 2012-13 में 24.5 फीसदी थी, वह 2013-14 में घटकर 20.59 फीसदी और 2014-15 में 15.23 फीसदी रह गई है।

बैंकों की तकनीकी भाषा में एनपीए वह कर्ज है जिसकी वापसी की किस्त देने में नब्बे दिन से ज्यादा की देरी हो गई हो। लेकिन बड़े कॉरपोरेट समूहों और उद्योगपतियों को दिए कर्ज के बड़े हिस्से के पुनर्भुगतान में देरी होने और डिफॉल्ट के बावजूद बैंक उसे एनपीए घोषित करने की बजाय कर्ज के भुगतान की किस्तों और भुगतान को पुनर्संरचित (री-स्ट्रक्चर) और पुनर्नियत (री-शेड्यूल) करते हैं। हालांकि यह कर्ज और उसका भुगतान मुश्किल में होता है और इससे बैंकों के मुनाफे और सेहत पर बुरा असर पड़ता है। यह एक तरह का खराब कर्ज ही है लेकिन इसे एनपीए घोषित नहीं किया जाता है। रिपोर्टों के मुताबिक, अगर ऐसे कर्जों को भी एनपीए में शामिल कर लिया जाए तो सरकारी बैकों का कुल एनपीए 9 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है।
सरकारी बैंक यानी नेताओं-कॉरपोरेट गठजोड़ की दुधारू गाय
आखिर सरकारी बैंकों का एनपीए इस तेजी से क्यों बढ़ा और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह सही है कि बैंकों के एनपीए में तेजी से बढ़ोतरी के पीछे एक वजह अर्थव्यवस्था की धीमी पड़ती रफ्तार खासकर मांग में आई गिरावट है। लेकिन यह स्थिति इसलिए भी पैदा हुई क्योंकि जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी तो बड़े कॉरपोरेट समूहों ने नए निवेश खासकर इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश के लिए मनमाने और अनाप-शनाप तरीके से कर्ज लिया। हालांकि यह बैंकों से लेकर कॉरपोरेट समूहों और सरकार सभी को पता है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र बहुत जोखिम भरा है। इसमें निवेश लंबे समय के लिए होता है और मुनाफा देरी से वापस आता है। इसके बावजूद प्रोजेक्ट के साथ जुड़े जोखिम को अनदेखा करते हुए बैंकों ने आंख मूंदकर कर्ज बांटा। पिछली सरकार ने जीडीपी की गति तेज करने और इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के नाम पर सरकारी बैंकों पर कर्ज देने के लिए दबाव बनाया और बड़े कॉरपोरेट समूहों ने बहती गंगा में खुलकर हाथ धोया।
बड़े कॉरपोरेट्स ने अपनी क्षमता से ज्यादा कर्ज लिया और उसे मनमाने तरीके से खर्च किया। कई बड़े कर्जदारों ने पैसे को इधर-उधर भी किया। मनी लॉन्डरिंग के जरिये विदेश भी ले गए और कई उसे पूरी तरह डकार कर बैठ गए। इसे ‘द ग्रेट इंडियन बैंक रोबरी’ कहना गलत नहीं होगा। निश्चित ही यह बैंक डकैती से कम नहीं है। इसमें बैंक के बड़े अधिकारियों से लेकर बड़े उद्योगपतियों, कॉरपोरेट समूहों और कारोबारियों की मिलीभगत साफ दिखाई देती है। लेकिन क्या यह सरकार में बैठे बड़े अधिकारियों और नेताओं के संरक्षण के बिना संभव है? सच यह है कि सरकारी बैंकों को गरीब की दुधारू गाय समझकर मनमाने तरीके से दूहा गया है। यह याराना पूंजीवाद का भी एक और उदाहरण है जिसमें सत्ता के करीबी उद्योगपतियों, कॉरपोरेट्स और कारोबारियों ने सरकारी बैंकों को अपने फायदे के लिए दुरुपयोग किया है। हैरानी की बात नहीं है कि विजय माल्या पर मचे शोर के बावजूद बैंकों और कॉरपोरेट्स के अधिकारियों और उद्योगपतियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय नहीं हो रही है।
चोर दरवाजे से बैकों के निजीकरण की तैयारी
मजे की बात यह है कि बैंकों की लूट में शामिल अधिकारियों और कॉरपोरेट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बजाय कॉरपोरेट स्पिन डॉक्टर पूरी बहस को चतुराई और सफाई से बैकों के निजीकरण की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी बहसों से लेकर गुलाबी अखबारों (आर्थिक अखबार) के संपादकीय और अर्थव्यवस्था के मैनेजरों की ओर से आ रहे संकेतों से साफ है कि वे सरकारी बैंकों के एनपीए के संकट को उनके निजीकरण के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनका तर्क है कि बैंकों की गड़बड़ियों की जड़ में सरकारी नियंत्रण है जिसका नेता और अफसर दुरुपयोग करते हैं। इसलिए बैंकों को सरकारी नियंत्रण से बाहर लाए और उन्हें निजी क्षेत्र के हवाले किए बिना समस्या हल नहीं होगी।
लेकिन बैंकों का निजीकरण बीमारी का इलाज नहीं बल्कि उसे लाइलाज बना देने का प्रस्ताव है। असल में, निजीकरण का तर्क देने वाले भूल जाते हैं कि अमेरिका में 2007-08 में डूबने वाले सभी बड़े बैंक निजी ही थे। अगर निजीकरण ही इलाज है और निजी प्रबंधन सबसे सक्षम है तो अमेरिकी बैंक क्यों डूबे? वे यह भी भूल जाते हैं कि भारत में 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले 1947 से 69 के बीच में कुल 559 निजी बैंक डूबे थे। लगता है कि 1991 के आर्थिक-वित्तीय सुधारों के बाद खूब धूमधाम से शुरू हुए निजी क्षेत्र के ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के डूबने का किस्सा भी वे भूल गए हैं। यही नहीं, वे यह भी नहीं बताते हैं कि 1969 से 2014 के बीच निजी क्षेत्र के कुल 23 बैंकों की वित्तीय स्थिति डगमगाने के बाद उन्हें सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ समाहित किया गया है।
देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी एक टिकाऊ और विश्वसनीय वित्तीय व्यवस्था को खड़ा करने में सरकारी बैंकों की केंद्रीय भूमिका है। सरकारी बैंकों की वित्तीय समावेशन यानी बैंकिंग सेवाओं को गांवों और गरीबों तक पहुंचाने और घाटे के बावजूद प्राथमिकता क्षेत्र जैसे कृषि और छोटे-लघु उद्योगों को कर्ज मुहैया कराने में अग्रणी भूमिका रही है। इन बैंकों के कारण ही भारत वैश्विक वित्तीय संकट की चपेट में आने से बच गया। इसके बावजूद बैंकों के निजीकरण की दुहाई क्यों दी जा रही है? यह किसी से छुपा नहीं है कि सरकारी बैंकों पर बड़े देसी कॉरपोरेट्स और विदेशी बैंकों की निगाह लगी हुई है।
सवाल यह है कि क्या एनडीए सरकार सरकारी बैंकों को कामकाज में वास्तविक स्वायत्तता देने, उनमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने, उन्हें जवाबदेह बनाने और सख्त निगरानी के दायरे में लाने की बजाय निजीकरण के शॉर्टकट के जरिये पूरी वित्तीय व्यवस्था को खतरे में डालने का जोखिम लेगी?